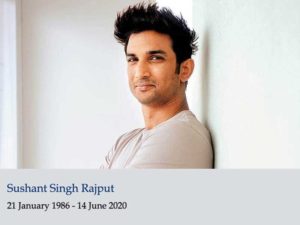रोज़ दिखती थी वह
रोज़ मिलती थी वह
चौराहे पे जैसे खो गई थी वह
अपना सदक़ा समझ कर
चंद पैसे दे कर
गाड़ी बढ़ा देता
ज़िन्दगी के रफ़्तार से
रफ़्तार मिला देता
पर उसकी हिजाबी आँखें
और उजरी क़बाएँ
कुछ और कहती थी
समझ न सका था मैं जो
समझना भी क्या था
ज़रुरतमंद थी वह
जब एक रोज़ पता चला
अय्याशों की मसली कहानी थी वह
सितम की मरी थी
पैसे नही हिफाज़त मांगती थी
इंसानी दरिंदों के चुंगल से
बचना चाहती थी वो
अफ़सोस किया, गाड़ी से उतरे
दूर तक निगाह दौड़ायी
शायद वक़्त के मानिन्द थी
फिर कभी मिली ही नही वह
~ रज़ा इलाही